पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार की उपस्थिति में ड्राफ्ट रेगुलेशन-2025 जारी किया। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी न्यूनतम अर्हता सुनिश्चित करने और उनकी सेवा शर्तों, शिक्षण एवं शोध कार्यभार, पेशेवर आचार संहिता आदि से संबंधित है। इस मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए शिक्षकों, शैक्षणिक प्रशासकों और छात्रों आदि हितधारकों को एक माह की समयसीमा दी गई है। देश में अभी तक रेगुलेशन-2018 को ही लागू करने की कवायद जारी है। इसलिए यह अवसर यूजीसी रेगुलेशन-2018 की विसंगतियों को दुरुस्त करने का था। उच्च शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी दृष्टि और नीतिगत निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। रेगुलेशन-2018 की विसंगतियों/समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए कई साल पहले एक समिति बनाई गई थी, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई प्रगति न होना निराशाजनक है।
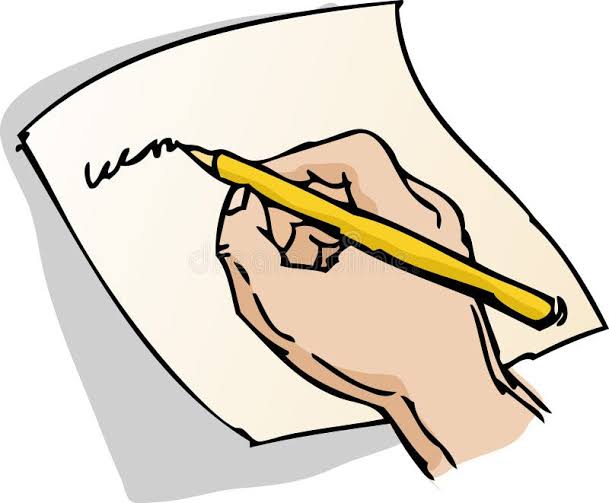
उक्त मसौदे में प्रतिभाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन का दावा तो है, लेकिन उसका कोई विश्वसनीय रोडमैप नहीं दिखता। ड्राफ्ट रेगुलेशन में शिक्षकों की नियुक्ति में स्नातक और स्नातकोत्तर के विषय की महत्ता घटाते हुए पीएचडी वाले विषयों में नियुक्ति की छूट दी गई है। यह निर्णय अकादमिक जगत में अराजकता बढ़ाएगा। यह विषय विशेष से पढ़े हुए अभ्यर्थियों को अन्य विषय में शिक्षक बनने का रास्ता खोलेगा। चार वर्षीय स्नातक करने वाले छात्रों को भी कालेजों/विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने का अवसर देने से भी अकादमिक गुणवत्ता घटेगी।
रेगुलेशन-2018 में विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता का प्रविधान किया गया था, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को अध्यापन से अधिक शोध कार्य करना होता है। अब पुस्तक के अध्यायों को शोध-पत्रों के समकक्ष दर्जा दे दिया गया है। यह चिंताजनक है। अभ्यर्थी की विभिन्न अकादमिक परीक्षाओं के अकादमिक परिणाम, शोध कार्य और प्रकाशन आदि को महत्व देने और साक्षात्कार की भूमिका
यूजीसी के नए ड्राफ्ट रेगुलेशन पर उठते सवाल फाइल
सीमित करने के संबंध में भी कोई पारदर्शी, वस्तुपरक और न्यायसंगत नीति नहीं बनाई गई है। चयन समिति केंद्रित नियुक्ति-प्रक्रिया को तो तोड़ा-मरोड़ा जाता रहा है। अभ्यर्थी की अकादमिक उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हुए अस्पष्ट और अमूर्त मानकों के आधार पर उसके मूल्यांकन का अधिकार चयन समिति को दिया गया है। अकादमिक उपलब्धियों संबंधी वस्तुपरक एवं सुपरिभाषित मानदंडों के स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया को चयन समिति केंद्रित बना दिया गया है। प्रकाशन की गुणवत्ता के निर्धारण से लेकर अंतिम चयन तक वही सर्वशक्तिमान होगी।
अकादमिक दुनिया जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और परिवारवाद से ग्रस्त है। संपर्कों संबंधों और लेन-देन के अभाव में योग्यतम अभ्यर्थी अनदेखी के शिकार होते हैं। यह स्थिति बदलनी होगी। अगर उच्च शिक्षा को बचाना है तो संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भारतीय उच्च शिक्षा सेवा शुरू की जानी चाहिए। केंद्रीय अनुदान प्राप्त सभी संस्थानों को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। इन सभी संस्थानों से रिक्तियों का विवरण मांगकर साल में एक बार विज्ञापन आना चाहिए और एक साथ लिखित परीक्षा और
अगर उच्च शिया को बचाना है तो संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भारतीय उच्च शिया सेवा शुरू की जानी चाहिए
साक्षात्कार होना चाहिए। नियुक्ति में 50 प्रतिशत अधिभार लिखित परीक्षा, 30 प्रतिशत अधिभार समस्त अकादमिक उपलब्धियों और 20 प्रतिशत अधिभार साक्षात्कार को दिया जाना चाहिए। सफल अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके स्थान, कालेज/विश्वविद्यालय को दी गई वरीयता और उसके स्थायी निवास स्थान आदि के समेकित अधिभार के आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। सत्र के बीच में कोई रिक्ति आने पर प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति की जानी चाहिए। यूजीसी से अनुदान प्राप्त सभी कालेजों के प्राचार्यों और सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति-प्रक्रिया को भी केंद्रीकृत करने की उ आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में सामाजिक न्याय के प्रविधानों का भी अनुपालन किया जाए।
ड्राफ्ट रेगुलेशन में कुलपति के रूप में शिक्षाविदों के अलावा उद्यमियों, प्रशासन पुलिस सेना के अधिकारियों, कंपनियों के प्रबंधकों आदि को चुनने की भी गुंजाइश है। इनके बजाय अकादमिक प्रशासन में अनुभवी संस्थान-निर्माताओं को ही कुलपति के रूप में चुना जाना चाहिए। संस्थान को विकसित करने वाले दृष्टिसंपन्न कुलपतियों के लिए भी कार्य समीक्षा के आधार पर दूसरे कार्यकाल का प्रविधान किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा क्षेत्र में तीन आयाम (वर्टिकल) बनाए जाने चाहिए-अध्यापन/शिक्षण, शोध/अनुसंधान और अकादमिक प्रशासन। शिक्षकों को करियर प्रारंभ करते ही प्रतिभा, योग्यता और अभिरुचि के आधार पर धीरे-धीरे इन तीन में से एक में प्रशिक्षित और विकसित किया जाना चाहिए। हमारे देश में अकादमिक प्रशासन को अत्यधिक हल्के में लिया जाता है और किसी भी आचार्य को प्राचार्य या कुलपति बनाने की रवायत है, जबकि अकादमिक प्रशासन अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। यह विशेषज्ञता, अनुभव और प्रशिक्षण की मांग करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के घोषित लक्ष्य के अनुरूप अगर भारत में अंतरराष्ट्रीय ख्याति के शिक्षण संस्थान विकसित करने हैं तो इस दिशा में दूरदर्शी नीति-निर्माण करना होगा
